गुरु विद्या देता है और अविद्या नष्ट करता है
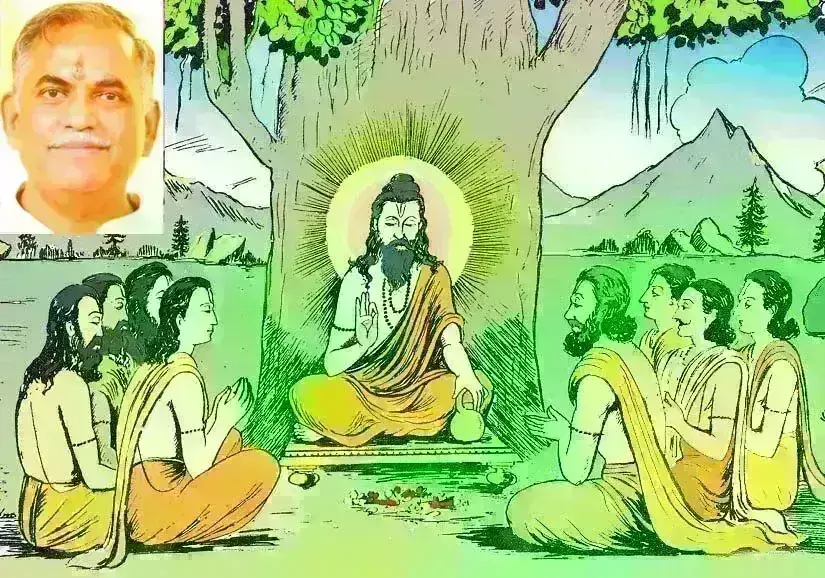
ओमप्रकाश श्रीवास्तव
जैसे शिक्षा व विद्या में अंतर होता है वैसे ही शिक्षक व गुरु भी अलग-अलग होते हैं। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो बुद्धि-विवेक को जाग्रत करती है। संसार में भले प्रकार से जीवन-यापन करने के लिए शिक्षा पहली आवश्यकता है। इसलिए जीवन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्या, शिक्षा से आगे की अवस्था है। व्यवस्थित, दोष रहित ज्ञान का नाम ही विद्या है। विद्या चरित्र गठन करती है - विद्या ददाति विनयं। विद्या प्रदान करना गुरु का दायित्व है। जो महान शिक्षक अपने आत्मानुभवों को उड़ेलकर छात्रों को सत्य का बोध कराने में सक्षम होते हैं, वह भी गुरुपद ग्रहण कर लेते हैं।
विद्या दो तरह की होती है अपरा विद्या और परा विद्या। मुण्ड कोपनिषद (1.1.4-5) में अंगिरा ऋषि कहते हैं कि जिससे लौकिक या पदार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो उसे अपरा विद्या कहा जाता है। चारों वेद, वेदांग आदि अपरा विद्या की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान का साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्रों, विज्ञान (साइंस) आदि भी अपरा विद्या की श्रेणी में आता है। छांदोग्य उपनिषद में कथा है कि नारदजी ने सनत्कुमार से उपदेश देने की प्रार्थना की। सनत्कुमार ने कहा पहले यह बताओ आप क्या जानते हो? नारद जी ने कहा कि मैंने चारों वेद, छहों वेदांग, इतिहास, पुराण, गणित, नाट्य शास्त्र, नृत्य, संगीत इत्यादि का भलीभांति अध्ययन किया है परन्तु मैं अभी तक आत्मा को नहीं जान पाया। सनत्कुमार ने कहा कि अपने जो सीखा है वह अपरा विद्या है, वह वाणी का विलास मात्र है। वाणी के श्रम से ब्रह्म नहीं मिल सकता। इनके आगे का मार्ग क्रियात्मिक साधना का है। अपराविद्या के बाद उसके अनुसार चलना शेष रहता है। वही परा विद्या है, जो मुक्त करा देती है-सा विद्या या विमुक्तये। वेदों में परा और अपरा दोनों विद्याएं समझाई गईं हैं। परा विद्या प्राप्त करने के लिए अंगिरा ऋषि की सलाह है कि-तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेवत्समित्पा णि: श्रोतियंब्रह्मनिष्ठम्। अर्थात् वेद को भली-भाँति जानने वाले, ब्रह्म में स्थित गुरु की शरण में जाना चाहिए। परम ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान या वेद वचनों से काम नहीं चलता उसके लिए वेदोक्त कर्म करना भी आवश्यक है। जो 'हैÓ अर्थात् सत्य या परमात्मा का बोध और जो 'नहीं हैÓ अर्थात् प्रकृति का निवारण कराने वाली युक्ति विद्या कहलाती है।
इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण शब्द है 'अविद्याÓ। अविद्या का अर्थ है किसी वस्तुत को वैसी समझना जैसी वह है ही नहीं। आचार्य शंकर के अनुसार पहले देखी हुई वस्तु की स्मृति छाया को दूसरी वस्तु पर आरोपित करना भ्रम है और यही अविद्या है। अंधकार में रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। इसका कारण अंधकार है। यह अंधकार ही अविद्या है। जब प्रकाश होता है तो पता चलता है कि वह तो रस्सी है। यह प्रकाश ही विद्या है। शिक्षा से जीवन में सुन्दरता आती है परन्तु उससे अविद्या का नाश नहीं होता। अविद्या का नाश विद्या से होता है। इस प्रकार जहाँ एक ओर शिक्षा व अपरा विद्या शास्त्रों, ग्रंथों में लिखी है शिक्षक या गुरु इन्हें प्रत्यक्षत: सिखाता है वही अविद्या और परा विद्या अमूर्त हैं। यह आंतरिक बोध की अवस्थाएं हैं।
जब हमें गलत बोध होता है तो उसका कारण अविद्या होती है। सीप की सफेद चमक में चांदी का आभास या रस्सी में साँप का भ्रम उत्पन्न होने पर हम उस वस्तु के मूल रूप को नहीं देख पाते हैं। अविद्या के कारण ही सांसारिक जीव, जगत् को सत्य मान लेता है और अपने वास्तविक रूप, ब्रह्म या आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। संसार का सारा आचार-व्यवहार एवं संबंध अविद्या से ग्रस्त संसार में ही संभव है। अविद्या न हो तो संसार का अस्तित्व ही संभव नहीं।
अविद्या के प्रभाव से नाशवान वस्तुओं को हम वास्तविक और अपना समझते हैं इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है और यही जन्म -मरण के बंधन का कारण है। ईशोपनिषद् में कहा है कि जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है - विद्यांचाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। अविद्ययामृत्युंतीर्त्वाविद्ययामृतमश्नुते॥ प्रकाश होते ही अंधेरे को हटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता वह स्वयमेव समाप्त हो जाता है इसी प्रकार विद्या के आते ही अविद्या से उत्पन्न भ्रम तत्क्षण समाप्त हो जाता है और बोध हो जाता है कि एकमात्र सत्य परमात्मा है संसार तो मिथ्या, माया है। माया, सर्वदेशीय भ्रम (ष्शह्यद्वद्बष् द्बद्यद्यह्वह्यद्बशठ्ठ) है तो अविद्या व्यक्तिगत अज्ञान (द्बठ्ठस्रद्ब1द्बस्रह्वड्डद्य द्बद्दठ्ठशह्म्ड्डठ्ठष्द्ग)।
गुरु का अर्थ है - जो अंधकार का नाश कर देता है। यह अंधकार अविद्या का है जो गुरु से प्राप्त होने वाली विद्या से नष्ट हो जाता है। गुरु, शिष्य को शिक्षा से शुरु करके पराविद्या के प्रकाश तक ले जाते हैं ताकि अविद्या का बोध समाप्त हो जाए और उसे जगत के पीछे के सत्यभान हो जाए। गुरु स्वयं में लक्ष्य नहीं है वह तो नाव की तरह है जिससे दरिया पार करना है। गुरु और शास्त्र पर श्रद्धा रखने से ही आगे का पथ प्रशस्त होता है। इस मार्ग में सात्विक श्रद्धा जितनी आवश्यक है, अंधश्रद्धा उतनी ही हानिकारक। आज के जमाने में गुरु को खोजना बहुत कठिन है क्योंकि तुलसीदास जी के शब्दों में कलियुग में 'पंडित सोइ जो गाल बजावाÓ 'जाकें नख अरु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकालाÓआदि की प्रधानता है। एक ओर श्रद्धाहीन होना जितना नुकसानदायक है दूसरी ओर उतनी ही नुकसानदायक सदैव संशय करने की आदत है। गीता में कहा है कि अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। 4.40।। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय करने वाले व्यक्ति का विनाश ही होता है। अत: गुरु को खोजना भी है, श्रद्धा भी रखनी है परंतु उसके पूर्व उसे अपने बुद्धि-विवेक की कसौटी पर कसना भी है।
गुरु से विद्या प्राप्ति के लिए शास्त्रों में तीन साधन बताये गये हैं- धन, जिज्ञासा और सेवा। गीता में इनका क्रम है -तद्विद्ध्प्रिणिपातेनपरिप्रश्नेहन सेवया।। 4.34।। अर्थात् पहले प्रणिपात अर्थात् विनम्रता, फिर परिप्रश्न अर्थात् जिज्ञासा और अंत में सेवा। गीता, शिक्षा की नहीं केवल विद्या की बात करती है इसलिए इसमें धन का उल्लेख नहीं है। यदि गुरु धन के बदले शिक्षा देता है तो एक ओर गुरु में स्वार्थ पैदा हो जाता है वहीं दूसरी ओर धन का कारण शिष्य में धनदाता होने के अहंकार के कारण शिक्षा प्राप्ति में बाधा आती है। धन से शिक्षा प्राप्त हो सकती है परंतु विद्या प्राप्ति संभव नहीं है। जब शिष्य प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है तो गुरु बिना किसी स्वार्थ के विद्या देता है इसलिए विद्या का संप्रेषण अधिक अच्छी तरह से होता है। तीसरा तरीका है सेवा और समर्पण का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है। सेवा में शिष्य में अंहकार नहीं होता और वह गुरु के सामने समर्पण कर देता है इसलिए वह गुरुवचनों को आत्मा से स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। वहीं गुरु में शिष्य के प्रति प्रेम व करुणा पैदा होती है इसलिए गुरु भी अपने सारे आत्मानुभव उड़ेल देता है। गीता में अर्जुन ने जब पूर्ण शिष्याभाव से समर्पण कर दिया- शिष्यदस्तेपह्यहंशाधि मां त्वां प्रपन्नम्।।।2.7।। तभी श्रीकृष्ण ने अपना उपदेश देना प्रारंभ किया।
गुरु कोई भी हो परंतु शिष्य को अपना विकास स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। गुरु से सीखने का अर्थ यह नहीं कि हम गुरु जैसे ही बन जाएं। हमारा अपना अस्तित्व अद्वितीय है। उसे पहचानें व गुरु की मदद से उसे विकसित करें। सच्चे गुरु प्रश्नों को हल करने का मार्ग बताते हैं वह उत्तर नहीं देते। उनका उत्तर तो शिष्य के लिए जानकारी होगी, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो तभी होगा जब शिष्य उस प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजेगा और प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। शास्त्रों में कहा है कि शिष्य को गुरु को नहीं खोजना पड़ता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। अगर आप अच्छे शिष्य हैं तो यह असंभव है कि आपको सद्गुरु न मिले। इसलिए यदि गुरु नहीं मिला है तो शिकायत मत करो यह देखो क्या तुम गुरु को आकर्षित करने के योग्य हो पाये हो? पहले आप शिष्य बनने की पात्रता तो विकसित करो फिर गुरु मिलेगा ही।
