अग्रलेख
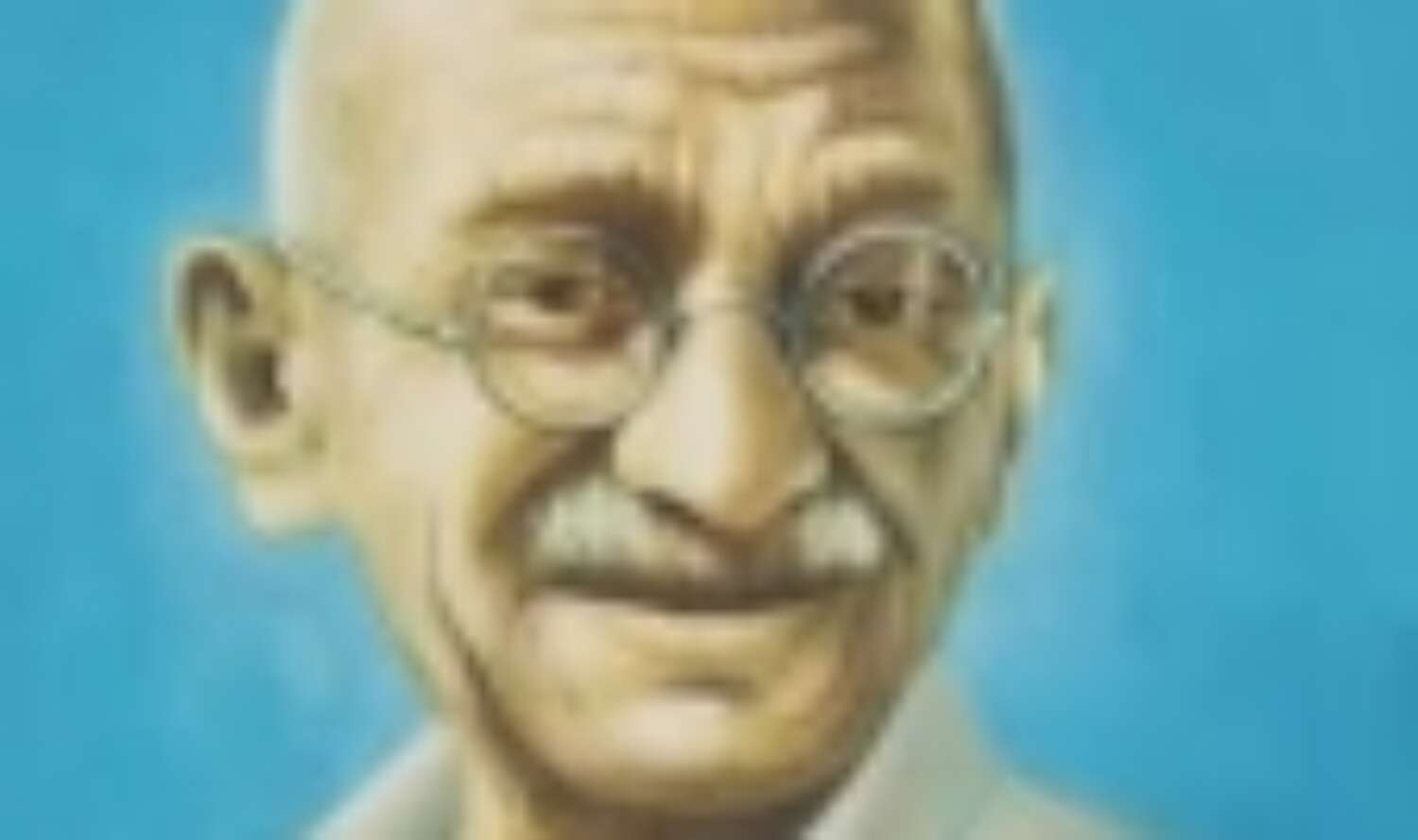
कहां है गांधी का हिन्द स्वराज्य?
- जयकृष्ण गौड़
महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को उनका स्मरण करते हैं, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधीजी की जीवनयात्रा 30 जनवरी 1948 तक चली। क्रूर हाथों से उनके जीवन का अंत हो गया। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका प्रवास में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, वहां से इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। उन्होंने हरिजन सहित कई समाचार पत्रों का संपादन किया। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। उन्होंने 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए प्रश्न और उत्तर के रूप में गुजराती में एक किताब लिखी, जिसका नाम दिया 'हिन्द स्वराज। स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी सभ्यता के आधार पर स्वदेशी अवधारणा के अनुकूल देश की उन्नति करे, विदेशी सभ्यता देश के लिए घातक है, इस प्रकार के विचार इस पुस्तक में व्यक्त किए गए हैं। इस पुस्तक के बारे में पं. जवाहरलाल नेहरू ने गांधीजी से कहा था कि 'हिन्द स्वराज मैंने पढ़ी है, इनमें दिए गए विचार की वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं रही। यह भी सब जानते है कि नेहरूजी पाश्चात सभ्यता से पूरी तरह रंगे हुए थे। जब नेहरूजी के नेतृत्व में 1947 में पहली सरकार बनी, उस समय विकास का पथ स्पष्ट नहीं था। संविधान की संरचना भी विदेशी संविधानों की नकल के आधार पर हुई। उस समय दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ सबसे अधिक विकसित और शक्तिशाली देश माने जाते थे। नेहरूजी दोनों से प्रभावित थे, कभी वे अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था के अनुरूप देश का विकास चाहते थे और कभी सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था के विकास मॉडल से प्रभावित थेबड़े उद्योग स्थापित होने से कुटीर एवं परंपरागत उद्योग समाप्त होने लगे, बेकारों की संख्या बढऩे लगी। खेत और किसान का कल्याण होने की बजाए शहरीकरण की ओर ध्यान दिया गया। गांधीजी ने स्वदेशी, खादी, चरखे पर जोर देकर देशी वस्तुओं के उपयोग की प्रेरणा दी। कांग्रेसियों की पहचान भी खादी के कपड़े और खादी की सफेद टोपी से होती थी। आज तो कांग्रेस से सफेद टोपी में इक्के दुक्के लोग दिखाई देते हैं। गांधीजी के विचारों के अनुरूप ही सर्वोदय का अभिमान चला। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई, सरदार पटेल आदि नेता गांधीजी के विचारों से प्रेरित थे। मुझे स्मरण है कि जब मोरारजी देसाई स्वदेश की नई मुद्रण मशीन का शुभारंभ करने इंदौर आए, तब मैं संवाददाता के नाते उनका संदेश प्राप्त करने इंदौर की रेसीडेंसी कोठी पहुंचा, वहां जब संदेश लेने लगा तो घड़ी देखकर एक दम रूक गए, मुझसे कहा कि चरखा चलाने का समय हो गया, बाद में शेष संदेश दे दूंगा। इस प्रकार चरखा और खादी का आग्रह गांधी के विचार से प्रभावित लोगों में रहा है। जब 1975 में इंदिराजी ने आपातकाल लगाकर गैर कांग्रेसियों के साथ जयप्रकाश नारायण समर्थक सर्वोदय कार्यकर्ताओं को भी मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। इंदौर के सर्वोदय आश्रम के प्रमुख दादाभाई नाईक जो उस समय करीब अस्सी वर्ष की आयु के थे, उन्हें भी जेल में बंद कर दिया था। दादाभाई, गांधीजी के स्वदेशी विचारों की प्रेरणा देते रहते थे। मुझे भी गांधीजी के विचारों को ठीक से समझने का अवसर जेल में दादाभाई के कारण मिला। गांधीजी ने 'हिन्दवी स्वराज में लिखा है कि 'हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए पर अंग्रेज नहीं चाहिए, आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह है कि आप हिन्दुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते है और हिन्दुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिन्दुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान बन जाएगा। यह मेरी सभ्यता का स्वराज नहीं है। गांधीजी ने यह भी लिखा है कि 'यूरोप की सभ्यता नुकसान देह है उससे यूरोप की प्रजा पामल (पागल) होती जा रही है। इस सभ्यता ने अंग्रेज प्रजा में सडऩ ने घर कर लिया है। यह सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली एवं स्वयं नाशवान है। इससे दूर रहना चाहिए। इसीलिए ब्रिटिश तथा दूसरी पार्लियामेंट बेकार हो गई है। गांधीजी ने भारतीय सभ्यता के बारे में लिखा है कि 'मैं मानता हूं कि जो सभ्यता हिन्दुस्तान की है, उस तक दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए है, उनकी बराबरी कर सके, ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आई। रोम मिट्टी में मिल गया। ग्रीस का सिर्फ नाम रह गया, मिश्र की बादशाही चली गई, जापान पश्चिम के शिकंजे में फंस गया और चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गिरा-टूटा जैसा भी हो, हिन्दुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत हैं। गांधीजी ने देश की भाषा हिन्दी है, उनका विचार था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के कारण ही बुराइयां पैदा हुई है। यह भी सच्चाई है कि गांधीजी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानजनक संबंध रहे। संघ के 'एकात्मता स्त्रोतÓ में गांधीजी का नाम है। संघ उन्हें प्रात: स्मरणीय मानता है। 25 दिसम्बर 1934 को गांधीजी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे। उनके साथ मीराबेन और महादेव देसाई थे। उसके बारे में गांधीजी ने कहा था कि मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ हूं। 12 सितम्बर 1947 को संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूज्य गुरुजी गांधीजी से मिलने बिरला हाउस गए थे। दोनों की संयुक्त अपील भी प्रकाशित हुई थी। १६ सितम्बर 1947 को दिल्ली की भंगी कालोनी में करीब पांच सौ स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए गांधीजी ने कहा था कि मैं तेरह वर्ष पूर्व वर्धा के संघ शिविर में गया था, जब संघ के संस्थापक जीवित थे। मैं वहां की अनुशासन भावना, अस्पृश्यता का सम्पूर्ण निषेध और सादगी से भरी नियमित दिनचर्या देखकर बहुत प्रभावित हुआ। कोई भी संगठन जो सेवा और आत्म बलिदान के ऊंचे आदर्शों से प्रेरित हो, वह अपनी शक्ति बढ़ाए बिना नहीं रह सकता। दुर्भाग्य यह रहा कि संघ पर गांधीजी की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया।
अब प्रश्न यह है कि गांधीजी जो भारत की सभ्यता के अनुरूप देश का कल्याण चाहते थे, जो धर्म संस्कृति आधारित स्वराज चाहते थे, उसके अनुरूप क्या देश का विकास पथ है? क्या स्वालंबन, आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी नीतियां निर्धारित होती है? क्या स्वभाषा में हमारा काम होता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं में ही मिलेगा। विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा हम आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। कुटीर उद्योग एवं परंपरागत उद्योगों को नष्ट किया जा रहा है। पाश्चात सभ्यता के जाल में फंसते जा रहे हैं। यदि गांधीजी के अनुरूप वर्तमान भारत की समीक्षा करे तो यह कह सकते हैं कि यह भारत का स्वराज नहीं, बल्कि पाश्चात सभ्यता की गुलामी में जकड़े जा रहे हैं।
यह मुहावरा प्रचलित है कि पराई थाली का भोजन ही अच्छा लगता है। इसी तरह हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिकी फार्मूले के अनुसार देश का विकास चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने रिटेल व्यापार में इक्कावन प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। क्या हम यह मानकर चलें कि गांधीजी के विचारों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, यदि ऐसा है तो यही कहा जाएगा कि गांधीजी के विचारों की हत्या कर दी है।
यदि गांधीजी के विचार नहीं रहे तो भारत अपने सांस्कृतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों से कट जाएगा। हमें गांधी के विचार को देश के लिए जीवित रखना होगा। गांधीजी के विचार ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार है। गांधी, संस्कृति, धर्म, राम और राष्ट्रीयता एक दूसरे के पर्याय है, इनके बिना भारत के वैभव का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।
