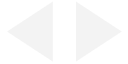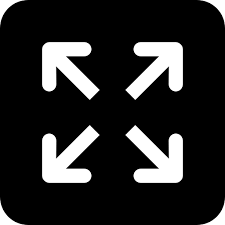हम स्वयं अपनी क्षमता को पहचानें
हम स्वयं से प्रेम नहीं करते। स्वयं के प्रति आत्मीय नहीं रहते। स्वयं से दूर ही रहते हैं बहुधा। हमारे पास स्वयं से परिचित होने का समय ही नहीं होता। हम सारी दुनिया की जानकारी प्राप्त करते हैं लेकिन स्वयं की जानकारी नहीं रखते। हम अपने अन्तर्जगत से अपरिचित रहते हैं। राग, द्वेष, प्रीति अप्रीति और हर्ष विषाद हमारे ही व्यक्तित्व के अंग हैं। हमारी प्रतिभा या कार्यकुशलता भी हमारे स्वयं का ही भाग होती है लेकिन स्वयं से ठीक परिचय न होने के कारण हम अपनी क्षमता की भी उपेक्षा करते हैं। हम अपने सम्बंध में भी दूसरों द्वारा दी गई जानकारियों पर विश्वास करते हैं। लेखन और राजनीति में दूसरों से प्राप्त सुखद जानकारियां प्राय: झूठी प्रशंसा होती हंै। राजनेता और लेखक के प्रशंसक उन्हें बड़ा बताते हैं। वे मान लेते हैं कोई दूसरा हमें छोटा बता देता है, हम उस पर खौरिया जाते हैं। हम अपने सम्बंध में भी सजग नहीं हैं। संसार में होना ‘एक गहन भाव’ है। अपने संदर्भ में इसे ‘स्वभाव’ कहते हैं। गीता के अनुसार ‘स्वभाव ही अध्यात्म’ कहा जाता है। संसार में हमारा होना हमारा चयन नहीं है। हम स्वयं की इच्छा से ही इस संसार में उपस्थित नहीं हैं। कारण कई होंगे। संसार जानना बेशक अच्छा ज्ञान है लेकिन स्वयं को जानने में ही संसार जानने के ऋजु मार्ग खुलते हैं।
स्वयं से प्रेम अनूठी प्रीति है। ऐसा कम होता है लेकिन हो तो कैसा रहेगा? प्रेम अस्तित्व का प्रसाद है। जीव चेतना की उच्चतम स्थिति है प्रेम। अस्तित्व भरा हुआ है प्रेम रस से। लेकिन प्रेम पंथ कठिन है। कठिनाई यही है कि प्रेम हमेशा दूसरे से होता है। अस्तित्व का प्रत्येक रूप आकार स्वयं से भिन्न है इसलिए दूसरा है। हम उसे प्रेम पाश में लाकर अपना बनाना चाहते हैं। प्रेम का अपना भाव है। वह दूसरे के प्रति प्रारम्भ तो हो सकता है लेकिन दूसरे के प्रति परवान नहीं चढ़ता। ऐसा प्रेम फल पकता नहीं, गंधमादन भी नहीं होता। इस प्रेमफल के भीतर अमृत रस नहीं होता। जब तक दूसरा उपस्थित है, तब तक प्रेम पूर्ण नहीं होता। प्रेम गली अति सांकरी ता में दुई न समाय। प्रेम में द्वैत नहीं। भक्ति प्रेम की ही अंतिम परिणिति है। यह प्रारम्भ होती है - दो से। एक भक्त और दूसरा भगवान। एक उपासक और दूसरा उपास्य। फिर चढ़ती है सारी मर्यादाएं तोडक़र। तब उपासक नहीं बचता, उपास्य में ही लीन हो जाता है। भक्त भगवान हो जाते हैं तब। भगवान भी कहां बचता होगा तब? तब सिर्फ भक्ति ही बचती होगी। भक्ति या प्रेम में द्वैत जरूरी है। सोचता हूं कि क्या प्रेम का अनुभव बिना दूसरे के भी संभव है? दूसरे के चक्कर में चक्कर लगाने से अच्छा है कि हम स्वयं को प्यार परिपूर्ण करें। प्रेम पकेगा, भक्ति पूर्ण होगी तो हम पूर्ण होंगे। पूर्णता की लब्धि का यह मार्ग सरल है।
गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का दर्शन है। गीता के कर्म पक्ष पर विद्वानों का ध्यान ज्यादा गया है। ऐसा उचित भी है। जीवन कर्म प्रधान है। ज्ञान का उपयोग भी कर्म में है। महाभारत के विदुर और श्रीकृष्ण दोनों ही परमज्ञानी हैं। विदुर नीति और ज्ञान की व्याख्या करते हैं तद्नुसार कर्म नहीं करते। श्रीकृष्ण कर्म, सांख्य ज्ञान और भक्ति के तत्व समझाते हैं। कर्म कुशलता को योग कहते हैं। श्रीकृष्ण का जीवन कर्मप्रधान है। ज्ञान के कारण उनके कर्म में फल की इच्छा नहीं है। वे भक्ति को भी चरम पर ले जाते हैं। गीता के अंतिम अध्याय (श्लोक 65) में भक्ति का चरम है। अर्जुन से कहते हैं-मन्मना भव भद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरू, मामेवैष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि में। कहते हैं - मुझमें मन लगा। मेरा भक्त बन। मेरे लिए यज्ञ कर। मुझे नमस्कार कर। इस तरह तू मुझे प्राप्त कर लेगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। क्या यह सब बोलने वाले गीता के प्रवक्ता मथुरा वाले साधारण श्रीकृष्ण ही हो सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति अपने मित्र से अपनी ही भक्ति के लिए ऐसे निर्देश दे सकता है? यहां श्रीकृष्ण अनुभूत भगवत्ता के प्रवक्ता हैं। वे इसीलिए अपनी भक्ति के निर्देश दे रहे हैं।
मैं अर्जुन जैसे अपने किसी मित्र को झंझट में नहीं डालूंगा। भक्ति और प्रेम के लिए दूसरे की जरूरत ही क्या है? अपनी सुविधा के लिए क्या मैं ऐसा ही निर्देश स्वयं को नहीं दे सकता? मैं स्वयं से कह सकता हूं - छोड़ो बेकार के काम, मेरा मनन करो। मेरा ही चिन्तन करो। मुझे ही प्यार करो। स्वयं को ही नमस्कार करो - मां नमस्कुरू। दूसरे की ओर मत देखो। ऋग्वेद के एक ऋषि वामदेव ने भी कहा था मैं ही उशना था, मैं ही कक्षीवान था, मेरी ओर देखो। मुझे जानो। स्वयं को स्वयं की ही भक्ति तरंगों में ले जाने का प्रयास निश्चित ही असाधारण है लेकिन जटिल नहीं। मेरे एक मित्र पूजा गृह में अपना एक बड़ा रंगीन चित्र लगाते थे। वे अपने चित्र के सामने बैठकर ध्यान करते थे। फूल और सुगंध भी अर्पित करते थे। वे मेरे द्वारा सम्पादित एक राजनैतिक पत्रिका के प्रबंध सम्पादक थे। मैंने यह दृश्य देखा। रहस्य पूछा तो बोले मेरे भीतर भी दिव्यता है, मैं उसी की प्राप्ति के लिए स्वयं की पूजा करता हूं। मैंने पूछा इसमें चित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उन्होंने कहा कि अपने चित्र में ध्यान लगाना आसान है। उनकी बात सही हो सकती है लेकिन मैं स्वयं को प्यार करने की धारणा रख रहा हूं। बेशक प्यार धारणा नहीं होता। यह विशिष्ट अन्तरभाव होता है। हम जिसे चाहने लगते हैं, उसके प्रति हमारे व्यक्तित्व से प्रेम तरंगों का प्रवाह होता है।
दो राय नहीं कि इस अस्तित्व में हरेक प्राणी सबसे ज्यादा स्वयं को ही प्यार करता है। यही प्राकृतिक भी है। हम दूसरों को भी अपने लिए ही प्यार करते हैं। वृहदारण्यक उपनिषद् के नायक दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को यही बात बताई थी। कहा था कि इस संसार में कोई किसी को प्यार नहीं करता। पत्नी पति को नहीं, पति पत्नी को नहीं। पुत्र पिता को नहीं। पिता पुत्र को नहीं। सब स्वयं को प्यार करते हैं। स्वयं की प्रीति में ही पिता, पुत्र को, पुत्र, पिता को, पत्नी पति को और पति, पत्नी को प्यार करते हैं। स्वयं को प्यार करना स्वाभाविक ही है लेकिन आधुनिक समाज स्वयं को नहीं स्वार्थ को प्यार करता है। स्वयं और स्वार्थ अलग-अलग तत्व हैं। स्वयं को प्यार करने वाले व्यक्ति की जीवन ऊर्जा बार-बार स्वयं पर लौटती है। जैसे समुद्र से उठे जलवाष्प आकाश में जाकर बार-बार धरती पर वर्षा करते हैं और समुद्र से बारंबार आकाशचारी होते हैं ठीक वैसे ही स्वयं को प्यार करने वाले की जीवन ऊर्जा स्वयं के भीतर से उठती है, अस्तित्व से रस लेती है, स्वयं पर ही बरसती है बार-बार। स्वार्थ में ऐसा नहीं होता। स्वार्थ में जीवन ऊर्जा का क्षय होता है। उपलब्धियां मन प्रशांत नहीं करतीं। जीवन विषाद से भरा रहता है।
स्वयं से प्यार में कोई द्विविधा नहीं। सुविधा ही सुविधा है। इस प्यार में हम ही आशिक हैं और हम ही माशूक। वैसे भी हम पूरे दिन स्वयं से ही लड़ते हैं। स्वयं से स्वयं की मुठभेड़ का प्रतिफल तनाव और उदासी में प्रकट होता है। हम नहीं चाहते कि किसी पुरस्कार, कर्मफल या लोभ में किसी सामान्य से याचना करें। फिर मन कहता है कि कर ही लें। मन द्विखंडित हो जाता है। पहले स्वयं से स्वयं के बीच अन्तर्विरोध और फिर याचना का अपमान। स्वयं से स्वयं की मुठभेड़ से स्वयं से स्वयं की प्रीति ज्यादा अच्छी है। स्वयं की गरिमा और महिमा की समझ का आनंद ही दूसरा है। स्वयं द्वारा स्वयं को नमस्कार और भी अच्छा। स्वयं के प्रति आत्मीयता प्राकृतिक अध्यात्म है और दूसरों के प्रति आत्मीयता का आचरण संस्कारजन्य अध्यात्मिकता। पहली सरल, तरल कविता है और दूसरी प्रयासपूर्वक जतन से गढ़ी गई वैचारिक स्थापना। स्व महत्वपूर्ण है, स्वयं ध्यान देने योग्य है। प्यार को नाम देने में बड़े-बड़े कल्पनाशील कवियों के सामने भी कठिनाई रही है। क्या स्वयं को स्वयं से प्यार करने की प्रीति को ‘सहज अध्यात्म’ नहीं कह सकते? ‘सहज योग’ की तरह।